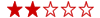ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना न तो आपको कुछ सिखाती है, और न ही आपका मनोरंजन करती है, सुकन्या वर्मा ने महसूस किया।

मुस्लिम सोशल जैसे भारी-भरकम टाइटल वाली इस फिल्म का नाम आओ, सेक्स की बात करें, बेबी भी हो सकता था।
ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना की छोटे से कस्बे में सेक्स क्लिनिक चलाने वाली अपनी मुख्य किरदार बेबी बेदी के माध्यम से सेक्स के मुद्दे पर खुल कर चर्चा करने की कोशिश तो बहुत ही नेक है।
लेकिन विकी डोनर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के इस क्षेत्र में डायरेक्टर शिल्पी दासगुप्ता की कमज़ोर कहानी और नाकाम कॉमिक टाइमिंग न तो आपको कुछ सिखाती है और न ही आपका मनोरंजन करती है।
हालांकि इसके परिस्थिति को दिखाने के अंदाज़ की तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना इस बात को बताने पर ज़्यादा ज़ोर देती है कि यह क्या है, न कि इसे क्या होना चाहिये।
हालांकि फिल्म का आधा समय उस समस्या के बारे में शर्मिंदग़ी महसूस करते हुए निकल जाता है, जिसका यह फिल्म समाधान करना चाहती है।
यह फिल्म मज़ेदार हो सकती थी, अगर लेखक गौतम मेहरा ने अपने ऐक्टर्स (अन्नू कपूर, राजेश शर्मा, वरुण शर्मा) के कॉमेडी के दायरे पर निर्भर न रहते हुए अपनी कुछ तीखी टिप्पणियों को इसमें शामिल किया होता।
स्पर्म की बोतल के पराठे पर गिरती घी में बदलने और टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में कहे गये शब्द 'मेक ड्राय वेट' और एक हास्यास्पद कोर्टरूम थर्ड ऐक्ट जैसे विज़ुअल गैग्स के बीच, ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना को कहीं कभी अपनी सही दिशा नहीं मिलती।
कहानी तब शुरू होती है जब फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिकल रिप्रेज़ेन्टिटिव और अपने परिवार की अकेली कमाऊ सदस्या बेबी बेदी (सोनाक्षी सिन्हा) अपने अंकल की अचानक मौत होने के बाद उनके सेक्स क्लिनिक की ज़िम्मेदारी उठा लेती है।
मालामाल और द बैचलर की तरह ही बेबी को भी अपनी किस्मत का पिटारा खोलने से पहले एक अजीब शर्त को पूरा करना होता है।
ये जो अंकल (कुलभूषण खरबंदा) हैं, एक हक़ीम और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट हैं -- जिन्हें सेक्शुअल (यौन) रोगों के अपने नुस्खे बताने के कारण एक बड़े मेडिकल इंस्टिट्यूट से निकाल दिया गया था -- और उन्होंने बेबी को यह क्लिनिक छः महीने तक चलाने के लिये कहा है, जिसके बाद वह क्लिनिक को बेच सकती है। ऐसा नहीं करने पर यह क्लिनिक कथित इंस्टिट्यूट की संपत्ति बन जायेगा।
जब ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना बेनेफ़िट-ऑफ़-डाउट की सीमाओं से बाहर चली जाती है, तो इसकी नाकाम कोशिशें और खोखली ख़ूबियाँ कहानी को बचा नहीं पातीं।
आँसू तो छोड़िये, अंकल की मौत की ख़बर से बेबी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आता। जैसे दोनों में कोई रिश्ता ही न हो।
लेकिन फिर शायद हमें ऐसा सोचने का मौका न देने के लिये दासगुप्ता ने बेबी के बचपन के कुछ फ़्लैशबैक्स के ज़रिये इस आदमी से बेबी के लगाव और उसके पदचिह्नों पर चलने की बेबी की कोशिश का कारण समझाने की कोशिश की है।
फिल्म में इस व्यक्ति को 'क़ुदरत के चुने हुए इंसान' की तरह दिखाया गया है, जिसके पीछे की ग़ैरज़िम्मेदार सोच की बात न ही की जाये तो बेहतर है। इस अयोग्य प्रैक्टिशनर को एक जन्मजात वैद्य की तरह दिखाया गया है, जिसके पास लोगों का चेहरा पढ़ कर उनकी बीमारी पहचान लेने की शक्तियाँ अपने आप आ गयी हैं, चॉकलैट में जूलियेट बिनोश के चॉकलेटियर की तरह।
इसी तरह का ऐल्फ्रेड मोलिना जैसा समाज का रक्षक बेबी को आगे बढ़ने से रोकता है।
यहाँ पर भी, ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना भेदभाव की उसी रीति को स्वीकार करने से दूर भागती है, जिसे समाज से मिटाने का यह दावा कर रही है।
हास्यास्पद बात है कि बेबी लोगों को अपनी बीमारियों को लेकर शर्मिंदा न होने के लिये कहती है, लेकिन कभी भी किसी की बीमारी को लेकर उसकी बेइज़्ज़ती करने से पीछे नहीं हटती। (आयुष्मान खुराना, क्यों न पाइल्स के लांछन पर अगली मूवी बनाई जाये?)
फिल्म की दुरंगी चाल के एक और उदाहरण के रूप में, बेबी का आलसी भाई (मज़ाकिया किरदार में वरुण शर्मा) एक होमोफोबिक (समलैंगिकता विरोधी) चुटकुला सुनाता है और फिर 'जागरुकता' के नाम पर उसे वापस ले लेता है।
और यह सब कुछ घोंघे की चाल से भी धीमी रफ़्तार से चलता है, जिसके कारण ख़ानदानी शाफ़ाख़ाना की ग़लतियाँ और उभर कर सामने आती हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से यह कई सब-प्लॉट्स को आगे बढ़ाता है, जिनसे कहानी को शायद ही कुछ मिल पाता है। ऐसा ही एक सब-प्लॉट है बेबी की माँ (नादिरा बब्बर, मिसेज़ बेनेट मोड की रानी) का, जो यूं तो खुली सोच रखती हैं लेकिन लेकिन एक दामाद के हाथों हुए अपने अपमान और बेटे की नालायकी को अनदेखा कर देती हैं।
या बेबी की ज़िंदग़ी में एक लेमोनेड मेकर (प्रियांश जोरे) के आने की बात को।
या फिर एक स्टार रैपर (बादशाह) की हक़ीक़त को, जिसके बाद उसका विचित्र हृदय परिवर्तन हो जाता है।
यह तो नहीं कहा जा सकता कि बादशाह का भड़कीला किरदार हमें जाने-अंजाने में हँसाता है, लेकिन कम से कम यह किरदार हमें 1990 के दशक की जूही चावला की सूझ-बूझ और लाजवाब अंदाज़ की कमी का एहसास दिलाने वाले सोनाक्षी सिन्हा के ग़ुस्सैल किरदार से थोड़ी राहत ज़रूर दिलाता है।
इतनी सारी बीमारियों से भरी कहानी को देख कर तो यही लगता है कि स्क्रिप्टराइटिंग के लिये भी एक शाफ़ाख़ाना ज़रूर होना चाहिये था।