उत्कर्ष मिश्रा के अनुसार फिल्म 'नो फादर्स इन कश्मीर' में कोई नायक या खलनायक नहीं है, केवल ऐसे असहाय चरित्र हैं, जिनके पास शायद उन चीज़ों के साथ ज़िन्दगी जीना सीखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिनके अधीन वे हैं।

ऐसी कुछ सुनी-सुनाई, तयशुदा कहानियाँ हैं, जो बाकी हिन्दुस्तान अक्सर कश्मीर के बारे में सुनता है।
सबसे पहले घेराबंदी और खोजबीन, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ होती है, और आगे चलकर ये आतंकवादियों और सैनिकों की मौतों में बदल जाती है; सुरक्षा कर्मियों पर गुस्सैल भीड़ द्वारा पत्थर फैंकना; आतंकवादियों का एकजुट होकर चेक पोस्ट या पुलिस स्टेशनों पर बम फैंकना, आदि-आदि...
इन सब बातों ने घाटी के बारे में कई पक्की धारणाओं को जन्म दिया है। लेकिन उनमें से सभी सही नहीं हैं।
ऑस्कर के लिए नामांकित निर्देशक अश्विन कुमार की फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर ऐसी ही एक रूढ़ोक्ति के साथ शुरू होती है।
नूर, जो एक ब्रिटिश किशोरी है और मूल रूप से कश्मीरी है, लंदन में अपने दोस्तों को बताती है कि वह अपनी जन्मभूमि पर जा रही है।
'देखो अगर तुम किसी आतंकवादी के साथ एक फोटो खिंचवा सको तो बहुत अच्छा होगा। वो तो कश्मीर में हर कहीं मिल जाएँगे - अल कायदा, तालिबान, आईएसआईएस...' उसकी दोस्त ने उससे कहा।
लेकिन कश्मीर में कई सनसनीखेज़ आश्चर्य उस लड़की के इंतज़ार में हैं, जिसका किरदार ज़ारा वेब ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है।
नूर के पिता, जो ब्रिटेन में पढ़े-लिखे एक कश्मीरी थे, वे कई साल पहले लापता हो गए थे।
नूर की माँ भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी के साथ अपना भविष्य तलाशने की कोशिश में है, और उसका अपने घर वापस जाना अपनी दूसरी शादी से पहले नूर के दादा-दादी से मिलने, और रिश्ते के उन आखिरी कमज़ोर धागों को मुकम्मल तौर पर काट देने की एक कोशिश है।
नूर हर कहीं नए-नए नज़ारों के फोटो खींचने में मसरूफ़ है और उसे उस झंझट का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, जिसमें वो पड़ने वाली है।
लेकिन इससे पहले वह एक स्थानीय लड़के माजिद से मिलती है, जो बड़ा मज़ेदार है। इस चरित्र को जीवंत किया है शिवम रैना ने।
माजिद एक आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाने की उसकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन वह उसे यह भी समझाता है कि एक उग्रवादी और एक आतंकवादी में क्या फ़र्क होता है।
नूर को पता चलता है कि उसके पिता की तरह माजिद के पिता भी लापता हो गए हैं। लेकिन वे उन्हें खुद छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सेना अपने साथ ले गई थी और वे फिर कभी नहीं लौटे।
माजिद अर्शिद से बड़ा प्रभावित है और वह उसकी तरह बनना चाहता है। इस चरित्र को खुद अश्विन कुमार ने निभाया है, जिसका व्यक्तित्व बड़ा संदेहास्पद और रहस्यमयी है। वह एक स्थानीय नेता है, एक अतिवादी अलगाववादी है, एक ऐसा आदमी है जो आतंकवादियों को छुपाता है, लेकिन जिसके संबंध सेना से भी हैं।
इन सबके साथ पता चलता है कि अर्शिद, नूर के पिता और माजिद के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। ज़ाहिर तौर पर अर्शिद ने सेना की असहनीय यातना से बचने के लिए उन्हें सेना को सौंप दिया था, जिसके कारण वह नपुंसक हो गया था। वह जानता है कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं।
नूर को ये गद्दारी लगती है और वह इसके लिए अर्शिद को धिक्कारती है। उसे एक राज़ मालूम था जो अब नूर भी जानती है।
उसके दादा-दादी, जिनके किरदार कुलभूषण खरबंदा और सोनी राजदान ने निभाए हैं, अर्शिद के बारे में सबकुछ जानते हैं, 'हालात को समझो', हालाँकि उसके दादा-दादी अर्शिद की कट्टरता और उसकी अलगाववादी सोच के लिए उसे अक्सर झिड़कते हैं।
नूर माजिद को उकसाती है कि वह उसके पिता की कब्र को ढूँढे, जो अर्शिद के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा के पास एक जंगल में है।
अपने मकसद में आगे बढ़ते हुए उसे एक और राज़ का पता चलता है और वह खुद को और माजिद को उस वक्त एक बड़ी मुसीबत में डाल देती है, जब उन्हें सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है।
यह कहानी कश्मीर घाटी में ज़िन्दगी के रोज़मर्रा के संघर्षों को बड़े तीखेपन के साथ पेश करती है, खास तौर पर उनकी ज़िन्दगी, जिनके बेटे, पति और पिता लापता हो गए हैं।
यह फिल्म ऐसे ही हज़ारों लोगों को 'समर्पित' है।
इस फिल्म में कोई नायक या खलनायक नहीं है, केवल ऐसे असहाय चरित्र हैं, जिनके पास शायद उन चीज़ों के साथ ज़िन्दगी जीना सीखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिनके अधीन वे हैं।
इसमें हमें कश्मीर में हो रहे टकराव के कई अलहदा रंग भी देखने को मिलते हैं। उनमें सभी बंदूक ताने आतंकवादी नहीं हैं और 'आज़ादी' के बारे में उनके विचार भी अलग है।
और अक्सर इन विचारों में टकराव होता है।
यह फिल्म स्व-घोषित स्वतंत्रता सेनानियों के पार जाती है, पत्थरबाज़ों के पार जाती है और एंकाउंटरों के भी पार जाती है, और हमें दिखाती है वो कश्मीर, जिसे हम यदा-कदा ही देख पाते हैं।
सेना के एक युवा मेजर के मुँह से निकले एक संवाद में हमें इस टकराव की जटिलता के सटीक दर्शन होते हैं, जिसमें वह कहता है कि 'मुझे उस जंग में जाना है जहाँ साफ़गोई हो, मुझे उस दुश्मन से मिलना है जिसे मैं साफ़-साफ़ देख सकूँ। यहाँ तो हर गाँव वाला, हर बाशिंदा एक दुश्मन है। मैं किसकी हिफ़ाज़त करूँ और किससे जंग लड़ू?'
नो फ़ादर्स इन कश्मीर को बड़ी ही खूबसूरती से फ़िल्माया गया है, जिसमें हमें बड़ी किफ़ायत के साथ कुदरत के स्वर्ग कश्मीर के दर्शन बड़ी समृद्धि से होते हैं। इसलिए सिनेमेटोग्राफी को पूरे अंक दिए जाते हैं।
इसकी पटकथा बड़ी सुगठित है, जो आने वाले हर दृष्य के प्रति हमें जिज्ञासू बनाए रखती है।
इस फ़िल्म में अपना कोई मत नहीं दिया गया है।
इसमें किसी भी पक्ष को महिमामंडित नहीं किया है, और न ही किसी को कमतर बताया गया है।
इसमें दर्शकों को अपने-अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।
इसलिए इसे किसी भी पूर्वाग्रह के बिना ही देखना चाहिए।
यह फिल्म न तो 2014 के बाद आए उन घोर-राष्ट्रवादियों के लिए है, जिनका सोचना है कि धारा 370 को हटाना ही एकमात्र समाधान है, और न ही उस 'आज़ादी' ब्रिगेड के लिए है, जिसे लगता है कि घाटी से सेना को रवाना कर देने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी।
हालाँकि इस फिल्म को आगे बढ़ने के लिए सेंसर के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, फिर भी इसमें ऐसे बहुत से वाकये हैं, जिन्हें देखने की उम्मीद आप आज के समय में नहीं कर सकते हैं।
वास्तव में इसके हर पहलू को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे बार-बार देखा जा सकता है।
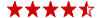












 © 2025
© 2025